Types of Input Device – इनपुट डिवाइस के प्रकार
इसके बहुत सारें प्रकार होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं-
- Keyboard
- Mouse
- Scanner
- Joystick
- Light Pen
- Digitizer
- Microphone
- MICR
- OCR
- Digital camera
- Paddle
- Steering wheel
- Touchpad
- Touchscreen
- Remote
- Webcam
1- Keyboard (कीबोर्ड क्या है?
यह एक basic इनपुट डिवाइस है जिसमे यूजर keys की मदद से कंप्यूटर को कमांड देता है।
इस डिवाइस में letters, numbers, characters, और functions जैसी keys मौजूद होती है जिन्हे दबाकर यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है।
यह डिवाइस USB और Bluetooth के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होते है।

Types of Keyboard – कीबोर्ड के प्रकार
इसके तीन प्रकार होते है :-
1- QWERTY Keyboard
यह एक modern कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड का उपयोग उन देशो में ज्यादा किया जाता है जो Latin-based alphabet का उपयोग नहीं करते।
इस कीबोर्ड का उपयोग आज के समय में सबसे ज्यादा किया जाता है।
2- AZERTY Keyboard
इस कीबोर्ड को फ्रांस के QWERTY layout के आधार पर डिज़ाइन किया गया है जिसे french keyboard भी कहा जाता है।
इस कीबोर्ड का उपयोग ज्यादातर France और European countries में किया जाता है।
3- DVORAK Keyboard
इस तरह के कीबोर्ड का इस्तेमाल typing speed बढ़ाने के लिए किया जाता है।
Features of Keyboard – कीबोर्ड की विशेषताएँ
1- कीबोर्ड का उपयोग mouse की जगह पर किया जा सकता है।
2- कीबोर्ड के चार primary component होते है – main keyboard, cursor keys, numeric keypad, और function keys.
3- यह डिवाइस expensive नहीं होते है।
2- Mouse (माउस क्या है?)
यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग cursor या pointer को स्क्रीन पर घुमाने (move) के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का प्रयोग flat surface पर किया जाता है।
mouse में left और right side में बटन होते है और इनके बिच में scroll wheel होता है। माउस का निर्माण वर्ष 1963 में Douglas C. Engelbart के द्वारा किया गया था।
यह डिवाइस wire और wireless तकनीक की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते है। हालांकि leptop में माउस का उपयोग नहीं किया जाता क्योकि इसमें पहले से ही touchpad मौजूद होता है जो मॉउस की तरह काम करता है।
यदि कोई यूजर लेपटॉप में माउस को कनेक्ट करना चाहता है तो वह आसानी से माउस को कनेक्ट कर सकता है।

Types of Mouse – माउस के प्रकार
इसके तीन प्रकार होते है :-
1- Trackball Mouse
इस माउस में cursor या pointer को move करने के लिए ball mechanism का उपयोग किया जाता है। ball mechanism बिलकुल गेंद (ball) की तरह होता है जिसकी मदद से स्क्रीन पर पॉइंटर को move किया जाता है।
इस बाल को finger , thump और palm (हथेली) की मदद से किसी भी डायरेक्शन में rotate या move किया जा सकता है।
2- Optical Mouse
यह एक ऑप्टिकल माउस है जो पॉइंटर को स्क्रीन पर घुमाने (move) के लिए optical electronics का उपयोग करता है।
यह माउस mechanical mouse की तुलना में अधिक विश्वसनीय (reliable) है और इसे ज्यादा maintain करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
इस माउस का उपयोफ flat surface पर किया जाता है।
3- Cordless or Wireless Mouse
इस माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए USB cable की ज़रूरत नहीं पड़ती।
यह माउस वायरलेस तकनीक radio, Bluetooth और Wi-Fi की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है।
Features of Mouse – माउस की विशेषताएँ
1- माउस का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को rotate करने के लिए किया जाता है।
2- इस डिवाइस का उपयोग करके यूजर एक साथ कई फाइल और फोल्डर को एक बार में select कर सकता है।
3- माउस का उपयोग फोल्डर , फाइल और किसी भी प्रोग्राम को open करने के लिए किया जाता है।
3- Scanner (स्कैनर क्या है?)
यह इनपुट डिवाइस image और documents को स्कैन करता है और इन्हे digital format में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद image और documents को कंप्यूटर स्क्रीन पर display करता है जिसे हम आउटपुट डेटा भी कह सकते है।
स्कैनर image और text फाइलों को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए (optical character recognition) तकनीक का प्रयोग करता है।
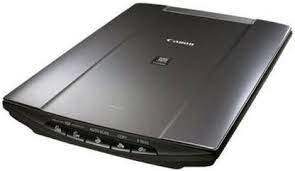
Types of Scanner – स्कैनर के प्रकार
इसके चार प्रकार होते है :-
1- Flatbed Scanner
यह एक प्रकार का स्कैनर है जिसमे एक glass pane और optical CIS और CCD मौजूद होता है। इस स्कैनर में image और documents को glass pane के ऊपर रखा जाता है और फाइलों को स्कैन किया जाता है।
इसके बाद स्कैनर फाइलों को copy करता है और उन फाइलों को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट। glass pane में एक तरह का प्रकाश (light) होता है जो फाइलों को स्कैन करने में मदद करता है।
2- Handheld Scanner
यह एक छोटा स्कैनर है जिसे हाथो में पकड़कर image को स्कैन किया जाता है। इस स्कैनर में किसी इमेज को स्कैन करते वक़्त हाथ बिलकुल स्थिर (stable) होने चाहिए।
3- Sheetfed Scanner
इस स्कैनर में एक slot होता है जिसमे documents को डाला जाता है। इस स्कैनर में (sheet-feeder, scanning module, और calibration sheet) जैसे component शामिल होते है।
इस स्कैनर का उपयोग single page वाले documents को स्कैन करने के लिए किया जाता है।
4- Photo Scanner
इस स्कैनर का उपयोग images को scan करने के लिए किया जाता है। इस स्कैनर में high resolution और color depth होता है जिसकी मदद से इमेज को स्कैन किया जाता है।
Features of scanner – स्कैनर की विशेषताएँ
1- स्कैनर low quality वाली images को भी स्कैन कर सकता है।
2- यह adaptable होते है जिसकी मदद से यूजर बड़े साइज वाले documents को स्कैन कर सकता है।
3- स्कैनर का उपयोग पुरानी तस्वीरों को साफ करने के लिए भी किया जाता है।
4- Joystick (जॉयस्टिक क्या है?)
joystick एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन के चारो तरफ cursor को rotate करने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस माउस की तरह होता है।
जॉयस्टिक में एक तरह की छड़ी (stick) होती है जिसकी मदद से कर्सर को किसी भी डायरेक्शन में move किया जा सकता है।
इस stick का उपयोग करके यूजर कर्सर को कण्ट्रोल करता है। joystick का निर्माण C. B. Mirick ने (U.S. Naval Research Laboratory) में किया था।
यह अलग अलग प्रकार की हो सकती है जैसे – (displacement joysticks, finger-operated joysticks, hand operated, और isometric joystick) .

Types of Joystick – जॉयस्टिक के प्रकार
इसके दो प्रकार होते है :-
1- Digital Joystick
digital joystick का उपयोग computer में किया जाता है। इस joystick को Atari-style के नाम से भी जाना जाता है।
2- Paddle joystick
इस joystick का उपयोग gamer के द्वारा game खेलने और गेम को कण्ट्रोल करने के लिए किया जाता है।
Features of Joysticks – जॉयस्टिक्स की विशेषताएँ
1- joystick का उपयोग कर्सर की position को कण्ट्रोल करने के लिए किया जाता है।
2- इसमें एक या एक से अधिक push button मौजूद होते है जिनको कंप्यूटर के द्वारा कण्ट्रोल किया जा सकता है।
5- Light Pen (लाइट पेन क्या है?)
यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका structure pen की तरह होता है। इस डिवाइस में एक प्रकार का detector होता है जिसकी मदद से यूजर स्क्रीन पर किसी object, file और program को choose कर सकता है।
इस डिवाइस का उपयोग LCD screen में नहीं किया जा सकता। इस pen का उपयोग करके यूजर स्क्रीन पर कुछ भी draw कर सकता है। light pen का निर्माण वर्ष 1995 में MIT (Massachusetts Institute of Technology) के द्वारा किया गया था।

Types of Light Pen – लाइट पेन के प्रकार
इसके दो प्रकार होते है :-
1- Led light pen
इस pen का उपयोग करते समय इसमें से एक चमकीली लाइट (bright light) निकलती है।
2- Design pen
इस pen का उपयोग स्क्रीन पर डिज़ाइन या स्केच बनाने के लिए किया जाता है।
Features of Light Pen – लाइट पेन की विशेषताएँ
1- यह pen ग्राफ़िक्स बनाते समय यूजर की मदद करते है।
2- इस pen की मदद से डिस्प्ले पर मौजूद objects को select किया जा सकता है।
6- Digitizer (डीजीटाइज़र क्या है?)
यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमे एक सपाट सतह (flat surface) होती है। इसमें एक pen होता है जो flat surface पर image और graphics बनाने में मदद करता है।
digitizer पर बनाये गए चित्र और ग्राफ़िक्स मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाई देते है। इस डिवाइस का उपयोग signatures , data और images को capture करने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा digitizer का उपयोग CAD (Computer-aided design) एप्लीकेशन और AutoCAD जैसे सॉफ्टवेयर को आउटपुट भेजने के लिए भी किया जाता है।
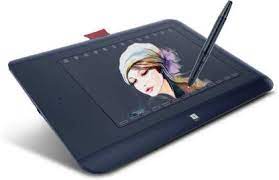
Features of Digitizer – डीजीटाइज़र की विशेषताएँ
1- इसमें एक pen होता है जो Drawing, writing और inserting जैसे कार्यो को पूरा करने में मदद करता है।
2- यूजर इस डिवाइस में touchscreen की तुलना में बेहतर तरीके से काम कर सकता है।
7- Microphone (माइक्रोफोन क्या है?)
microphone एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ध्वनि (sound) को इनपुट में बदलने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का उपयोग करके यूजर ध्वनि (sound) के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट डेटा भेजता है।
यह डिवाइस sound vibration को audio signal में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ऑडियो सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके उस डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर देता है।
microphone का उपयोग presentation में sound को add करने और webcam में video conferencing करने के लिए किया जाता है। एक microphone तीन तरीको से audio waves को कैप्चर कर सकता है .

Features of Microphone in Hindi – माइक्रोफोन की विशेषताएँ
1- microphone में एक प्रकार का diaphragm होता है जिसमे Sound waves टकराती है।
2- जब यूजर microphone में कुछ बोलता है तब diaphragm vibrate करता है।
8- MICR (MICR क्या है?)
MICR का पूरा नाम (Magnetic Ink Character Recognition) है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग magnetic ink से लिखे गए text को read करने के लिए किया जाता है।
इस डिवाइस का उपयोग bank और organisation में cheques को जांचने (check) के लिए किया जाता है। यह डिवाइस एक मिनट में 300 cheques को जांच सकता है।
cheques के निचे लिखा गया MICR नंबर magnetic ink से लिखा जाता है। magnetic ink बनाने के लिए MICR toner के साथ laser printer का प्रयोग किया जाता है।

Features of MICR – MICR की विशेषताएँ
1- यह एक character recognition तकनीक है जो cheques की जाँच करती है।
2- यह डिवाइस bank और organisation में सुरक्षा (security) को बढ़ाने में मदद करता है।
3- यह डिवाइस बैंक में होने वाले fraud से बचाता है।
9- OCR (OCR क्या है?)
OCR का पूरा नाम (Optical Character Reader) है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हाथ से लिखे गए टेक्स्ट (handwriting) को digital text में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा OCR का उपयोग documents और books को electronic files में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है।
यह डिवाइस hard copy और historic documents को PDF files में कन्वर्ट करने में मदद करता है।
यह डिवाइस स्कैनर का उपयोग करके document को copy करता है।

Features of OCR – OCR की विशेषताएँ
1- यह डिवाइस Character को identify करने में सक्षम है।
2- इस डिवाइस का output फाइल का फॉर्मेट (Word, Excel, PDF, eBook) होता है।
10- Digital camera (डिजिटल कैमरा क्या है?)
यह एक डिजिटल डिवाइस है जो image को capture करता है और वीडियो को रिकॉर्ड करता है।
कैप्चर की गई इमेज और रिकॉर्ड की गई वीडियो फाइल को यह मेमोरी में स्टोर करता है।
इस डिवाइस में images को capture करने के लिए sensor chip का प्रयोग किया जाता है।
इस डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है जिसे हम डिजिटल कैमरा भी कहते है।

Features of Digital Camera – डिजिटल कैमरा की विशेषताएँ
1- इस डिवाइस की मदद से black and white इमेज बनाई जा सकती है।
2- इस डिवाइस में images को किसी भी डायरेक्शन में move या rotate किया जा सकता है।
11- Paddle (पैडल क्या है?)
यह एक साधारण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग gamers के द्वारा game खेलते वक़्त किया जाता है। इस डिवाइस का structure पहिये (wheel) की तरह होता है जिसे हाथो से पकड़ा जाता है।
इस डिवाइस का उपयोग volume को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है।
यह डिवाइस खेल के दौरान कर्सर या किसी वस्तु (object) को कण्ट्रोल कर सकता है। हम इस डिवाइस का उपयोग joystick की जगह पर कर सकते है।

Features of Paddle – पैडल की विशेषताएँ
1- इस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर के functions को कण्ट्रोल किया जा सकता है।
2- इस डिवाइस का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी किया जाता है।
12- Steering wheel (स्टीयरिंग व्हील क्या है?)
यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग racing video games जैसे – (car racing games) में किया जाता है।
यह एक driving program है जो gamer को वाहन (vehicle) को चलाने में मदद करता है।
इस डिवाइस में एक steering wheel होता है जो वाहन को left और right side move करने में मदद करता है।
इस डिवाइस में acceleration , brake pedal और shifting gears होता है जो पुरे वाहन को कण्ट्रोल करने में मदद करता है।

Features of Steering wheel – स्टीयरिंग व्हील की विशेषताएँ
1- इस डिवाइस का उपयोग करके यूजर car driving का अनुभव (experience) ले सकता है।
2- यह डिवाइस expensive होते है।
13- Touchpad (टचपैड क्या है?)
touchpad एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग mouse के स्थान पर किया जाता है। टचपैड का उपयोग लेपटॉप में किया जाता है।
इस डिवाइस में यूजर अपनी उंगलियों की मदद से कर्सर या पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है।
माउस की तरह ही इसमें left और right में बटन होते है जो किसी ऑब्जेक्ट को click करने में मदद करते है।
इस डिवाइस का उपयोग करके यूजर object को select कर सकता है , किसी प्रोग्राम को open कर सकता है , किसी फाइल को delete कर सकता है। ऐसे बहुत से काम है जिनको यूजर कर सकता है।

Features of Touchpad – टचपैड की विशेषताएँ
1- इस डिवाइस में यूजर अपनी उंगलियों की मदद से कर्सर को rotate करता है।
2- माउस की तुलना में यह ज्यादा user friendly होते है।
14- Touchscreen (टचस्क्रींन क्या है?)
Touch screen का उपयोग ज्यादतर smartphone और tablet जैसे devices में किया जाता है। इसमें यूजर अपनी उंगलियों की मदद से डिवाइस को कण्ट्रोल करता है या फिर कहे इनपुट देता है।
यूजर अपनी उंगलियों की मदद से डिवाइस के किसी भी function को open कर सकता है। जैसे phone को unlock करना , email खोलना , app खोलना और फाइलें खोलना। touchscreen का निर्माण पहली बार वर्ष 1965 में E.A. Johnson के द्वारा किया गया था।
पहली touchscreen को वर्ष 1970 के दशक में CERN के engineer Frank Beck और Bent Stumpe के द्वारा लांच किया गया था।

Features of Touchscreen – टचस्क्रींन की विशेषताएँ
1- touchscreen का उपयोग करना आसान है।
2- इसमें यूजर को higher resolution मिलता है।
15- Remote (रिमोट क्या है?)
यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका निर्माण डिवाइस के functions को कण्ट्रोल करने के लिए किया गया है।
इसका सबसे अच्छा उदहारण T.V. remote है जिसका उपयोग चैनल बदलने , वॉल्यूम को घटाने और बढ़ाने , T.V. को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है।
रिमोट का निर्माण वर्ष 1956 में Dr. Robert Adler of Zenith के द्वारा किया गया था। यह devices को कमांड देने के लिए electromagnetic waves भेजता है।

Features of Remote – रिमोट की विशेषताएँ
1- रिमोट को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है।
2- इस डिवाइस का उपयोग करना आसान है।
16- Webcam (वेबकेम क्या है?)
webcam एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यह डिवाइस इमेज को कैप्चर कर सकता है और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।
यह डिवाइस कैप्चर की गई images और video को कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर सकता है।
यह बिलकुल डिजिटल कैमरा की तरह ही काम करता है।

Features of Webcam – वेबकैम की विशेषताएँ
1- यह कैमरा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है।
2- इस कैमरे में light quality कम होती है।
Types of Output Device – आउटपुट डिवाइस के प्रकार
इसके बहुत सारें प्रकार होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं-
- Monitor (मॉनिटर)
- Printer (प्रिंटर)
- Plotter (प्लॉटर)
- Projector (प्रोजेक्टर)
- Speaker (स्पीकर)
- Headphone (हैडफ़ोन)
- Sound Card (साउंड कार्ड)
- Video Card (विडियो कार्ड)
- GPS (जीपीएस)
- Speech Synthesizer (स्पीच सिंथेसाइज़र)
Monitor (मॉनिटर क्या है?)
- मॉनिटर कंप्यूटर का एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। इसे कभी-कभी visual display unit (VDU) भी कहा जाता है।
- मॉनिटर वीडियो, ऑडियो, इमेज और text को कंप्यूटर में दिखाता है।
- यह एक TV की तरह ही होता है परंतु इसका resolution टेलीविज़न (TV) से अधिक होता है।
- 1 मार्च 1963 को सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर को विकसित किया गया था।
- जब monitor किसी डाटा को अपनी screen में डिस्प्ले करता है तो उस डाटा को pixel के रूप में जाना जाता है।

मॉनिटर के प्रकार
मॉनिटर 6 प्रकार के होते हैं –
- Cathode Ray Tube (CRT) Monitor
- Flat Panel Monitor
- Touch screen monitor
- LED Monitor
- OLED Monitor
- DLP Monitor
1 – Cathode Ray Tube (CRT) Monitors –
CRT Monitor स्क्रीन पर चित्र को दिखाने के लिए electronic beam का इस्तेमाल करते है। इस इलेक्ट्रॉनिक बीम के अंदर एक प्रकार की gun (बंदूक) होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक किरणों को आग लगाने में मदद करती है। जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक किरणे मॉनिटर की सतह पर बार बार टकराती है।
इलेक्ट्रॉनिक किरणों के सतह पर टकराने की वजह से मॉनिटर में अलग-अलग प्रकार के रंग पैदा होते है और इन्ही रंगो के कारण मॉनिटर में इमेज या वीडियो display होती है।
2. Flat Panel Monitors
फ्लैट पैनल मॉनिटर में बहुत ही पतले (Thin) पैनल का इस्तेमाल किया जाता है।
ये मॉनिटर वजन में काफी हल्के होते है और इनको रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। हल्के होने की वजह से इस मॉनिटर को हम अपने साथ कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं।
CRT मॉनिटर की तुलना में flat panel monitor बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं।
ये मॉनिटर रेडिएशन (radiation) के मामले में भी काफी अच्छे होते है। क्योकि ये नुकसान दायक radiation उत्पन्न नहीं करते।
CRT की तुलना में ये monitor थोड़े महंगे होते है।
फ्लैट पैनल मॉनिटर का उपयोग TV,, computer, और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में किया जाता है।
3– Touch Screen Monitors
टच स्क्रीन मॉनिटर को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में जाना जाता है। क्योकि टच स्क्रीन मॉनिटर में हम बिना किसी keyboard और mouse के कंप्यूटर को input दे सकते है।
इस मॉनिटर में हम स्क्रीन को touch करके किसी भी program को आसानी से open कर सकते है और फिर उसमें काम कर सकते हैं।
4 – LED Monitors
LED monitor फ्लैट पैनल मॉनिटर की तरह वजन में हल्के होते है।
LED monitor का उपयोग लैपटॉप, मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, और टैबलेट के लिए किया जाता है।
इसका अविष्कार James P. Mitchell ने किया था। इसके अलावा यह ज्यादा expensive (महंगा) नहीं होता। इसको maintain करके रखना काफी ज्यादा आसान होता है।
5 – OLED Monitors
OLED का पूरा नाम Organic Light Emitting Diode है। OLED मॉनिटर एक नया मॉनिटर है जिसमें बहुत अच्छे Color दिखते हैं और यह मॉनिटर बहुत पतला होता है।
यह मॉनिटर यूज़र को एक बेहतर experience देता है। इसका उपयोग smartphone और tablet की स्क्रीन बनाने के लिए किया जाता है।
6– DLP Monitor
DLP monitor को डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। DLP monitor का इस्तेमाल बड़ी स्क्रीन में चित्रों को display करने के लिए किया जाता है।
शुरुआती दौर में DLP बड़ी स्क्रीन में चित्रों को धुँधला दिखाया करती थी। क्योकि उस समय DLP में LCD का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल DLP बड़ी स्क्रीन में चित्रों को display करने के लिए micromirror device का इस्तेमाल करती है।
मॉनिटर के फायदे –
इसके फायदे निम्नलिखित हैं-
- आजकल ऐसे मॉनिटर आ गए हैं जो बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं।
- इसके द्वारा यूज़र किसी भी चीज़ को देखकर आसानी से समझ सकता है।
मॉनिटर के नुकसान –
- कुछ ऐसे monitor होते हैं जो radiation (रेडिएशन) पैदा करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
- कुछ monitors को maintain करके रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है।
- मॉनिटर का price (मूल्य) ज्यादा होता है।
- मॉनिटर को रखने के लिए ज्यादा space (जगह) की जरूरत होती है।
Printer (प्रिंटर क्या है?)
- प्रिंटर एक output device है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में मौजूद text और image को कागज में प्रिंट कर सकते हैं।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर की soft copy को hard copy में बदलने का काम करता है।
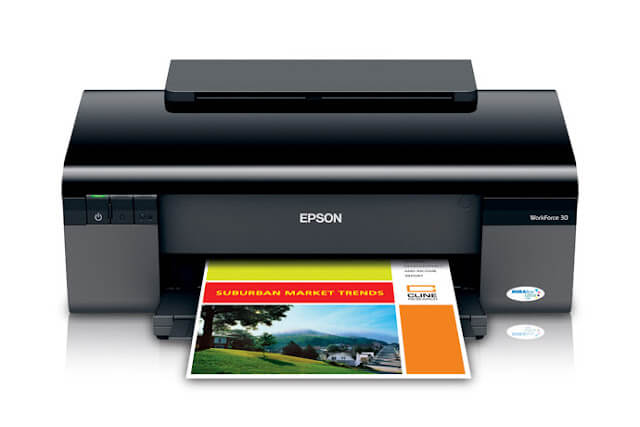
प्रिंटर के प्रकार
प्रिंटर के 5 प्रकार होते हैं –
1 – Laser Printer (लेज़र प्रिंटर)
Laser printer का इस्तेमाल कागज में text और images को प्रिंट करने के लिए किया जाता है।
लेज़र प्रिंटर कागज में text और images प्रिंट करने के लिए laser light का इस्तेमाल करता है।
लेज़र प्रिंटर के अंदर सिलिंडर के आकार का एक drum मौजूद होता है।जिस ड्रम को Photoreceptor के रूप में जाना जाता है।
2 – Photo printer (फ़ोटो प्रिंटर)
Photo printer के द्वारा बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की डिजिटल फ़ोटो को प्रिंट कर सकते हैं।
इसका इस्तेमाल photo paper के ऊपर फ़ोटो को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फोटो पेपर दिखने में बिलकुल सफेद रंग के होते है।
Photo printer में इस्तेमाल किये जाने वाले फोटो पेपर के ऊपर एक लेयर होती है। जो बिलकुल oily (चिकनी) होती है। फोटो प्रिंटर के द्वारा सभी आकार की फ़ोटो को प्रिंट किया जा सकता है।
3- Color Printer (कलर प्रिंटर)
कलर प्रिंटर CMYK कलर मॉडल पर आधारित होता है। CMYK कलर मॉडल के अंदर चार प्रकार के रंग शामिल होते है – Cyan (सियान), Magenta (मजेंटा), Yellow (पीला) और Black (काला).
CMYK मॉडल इन सभी रंगो को एक दूसरे के साथ प्रिंट करता है। कलर प्रिंटर एक से ज्यादा रंगो को प्रिंट करने की क्षमता रखते है।
Color printer का इस्तेमाल ज्यादातर किताबो , कागज सामग्री और पत्रिकाओं की छपाई के लिए किया जाता है।
4- Inkjet Printer (इंकजेट प्रिंटर)
इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें किसी कागज में print करने के लिए ink (स्याही) का इस्तेमाल किया जाता है।
इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल हाई क्वालिटी छपाई के लिए किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर output देने में ज्यादा समय का वक़्त नहीं लगाते है। इंकजेट प्रिंटर ज्यादा expensive (महँगे) नहीं होते।
5- Digital Printer (डिजिटल प्रिंटर)
डिजिटल प्रिंटर का इस्तेमाल डिजिटल फाइल्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जो फाइल TIFF, PDF etc के फॉर्मेट में होती है।
डिजिटल प्रिंटर में printing plate की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटल प्रिंटर paper, fabric, canvas, और cardstock पर डाटा को सीधे प्रिंट कर देता है।
डिजिटल प्रिंटर का उपयोग दूकान , बिज़नेस कार्ड , और letterheads के लिए किया जाता है।
Advantages of Printer in Hindi – प्रिंटर के फायदे
- प्रिंटर की मदद से data को हार्डकॉपी में print कर सकते है।
- यह text, फ़ोटो और ग्राफिवस को किसी भी size में प्रिंट करने की छमता रखता है।
- इसकी मदद से डाटा को आसानी से समझा और पढ़ा जा सकता है।
Disadvantage of Printer in Hindi – प्रिंटर के नुकसान
- प्रिंटर काफी ज्यादा expensive (महँगे) होते है। इसके अलावा प्रिंटर को maintain करके रखने में काफी ज्यादा पैसे खर्च होते है।
- इसमें पेपर waste (बर्बाद) भी होता है। क्योकि इसके द्वारा कुछ डाटा सही तरीके से प्रिंट नहीं हो पाता। जिसकी वजह से पेपर के बर्बाद होने का खतरा बना रहता है।
Plotter (प्लॉटर क्या है?)
- प्लॉटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो high quality के ग्राफ़िक्स को प्रिंट करने में मदद करता है।
- Plotter के अंदर अलग अलग प्रकार के रंग होते है।
- प्लॉटर printer की तरह ही काम करता है। लेकिन इसमें हाई क्वालिटी के ग्राफ़िक्स को प्रिंट करने की छमता होती है।
- इसके अलावा plotter का इस्तेमाल 3D पोस्टर , 3D इमेज , 3D डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है।

Types of Plotter – प्लॉटर के प्रकार
1 – Drum Plotter (ड्रम प्लॉटर)
Drum plotter को roller plotter भी कहते हैं। इसमें एक drum या roller होता है जिसमें paper (कागज़) को रखा जाता है।
इसमें drum कागज को दायीं और बायीं तरफ घुमाता है। परन्तु इसमें प्रिंटिंग का काम pen करती है।
2 – Flat Bed Plotters
Flat bed plotter एक ऐसा ग्राफ़िक्स प्लॉटर है जिसमें कागज को flat surface (सपाट सतह) पर रखा जाता है। इसमें surface का size जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा drawing का साइज होगा।
कुछ flatbed plotter ऐसे होते है जो पेपर की बजाय कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और metal (धातु) में भी प्रिंट करते हैं।
इसमें graphics और pictures को draw करने के लिए pen का इस्तेमाल किया जाता है।
Flat bed plotter का इस्तेमाल चमकदार और रगीन ग्राफ़िक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसमें अलग-अलग रंगो का इस्तेमाल किया जाता है।
3 – Ink Jet Plotters
Inkjet plotter सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्लॉटर है। इसकी खासियत यह है कि इसमें high quality में प्रिंट कर सकते हैं।
इस प्लॉटर में, image या graphics को प्रिंट करने के लिए कागज में ink की छोटी-छोटी बूंदे डाली जाती है।
इस प्लॉटर का इस्तेमाल बहुत बड़े-बड़े banner और billboard को बनाने के लिए किया जाता है।
इंकजेट प्लॉटर में प्रिंटिंग के लिए चार रंगो (Cyan, magenta, yellow और black) का इस्तेमाल किया जाता है। क्योकि इंकजेट प्लॉटर के पास चार प्रकार के कलर ही उपलब्ध है।
इंकजेट प्लॉटर की स्याही बिलकुल पानी की तरह पतली होती है। जिसके कारण प्रिंटिंग करते वक़्त कागज ज्यादा भारी नहीं होता। कहने का मतलब है की स्याही बिलकुल हल्की होती है जिसके कारण प्रिंट की हुई चीज़ कागज के उपर बिलकुल हल्के हो जाते है।
Advantage of Plotter – प्लॉटर के फायदे
- प्लॉटर high quality के ग्राफ़िक्स और image बनाने में मदद करता है।
- यह उच्च स्तर का resolution प्रदान करता है।
- इसमें यूजर को ग्राफ़िक्स या इमेज प्रिंट करने के लिए ज्यादा option मिल जाते है।
Disadvantage of Plotter – प्लॉटर के नुकसान
- इसमें मैमोरी बहुत कम होती है।
- printer की तुलना में plotter काफी ज्यादा expensive (महँगे) होते है।
Projector (प्रोजेक्टर क्या है?)
- Projector एक तरह का output डिवाइस है जो वीडियो या चित्र को बड़े स्क्रीन या दीवार में display करने में मदद करता है।
- सरल शब्दो में कहे तो “प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम वीडियो या इमेज को बहुत बड़े साइज में दिखा सकते है।”
- इसका इस्तेमाल कॉलेज में बहुत सारें students को पढ़ाने के लिए किया जाता है। जिससे कि सारें students वीडियो को देख पाए।

Types of projector – प्रोजेक्टर के प्रकार
1. 4K projector
4K प्रोजेक्टर की मांग मार्किट में सबसे ज्यादा होती है। क्योकि यह प्रोजेक्टर काफी ज्यादा लोकप्रिय होते है।
4K projector को Bluetooth, Wi-Fi, और USB की मदद से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है।
4K प्रोजेक्टर DLP टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके अलावा इन प्रोजेक्टर का वजन लगभग 865 ग्राम के आस पास होता है। 4K projector को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती।
2.LED projector
LED projector को मोबाइल , लेपटॉप जैसे डिवाइस के साथ आसानी से connect किया जा सकता है।
LED प्रोजेक्टर स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए LED लाइट का इस्तेमाल करते है। जिसके कारण इमेज और वीडियो high quality की दिखाई देती है।
इसके अलावा LED प्रोजेक्टर को remote के द्वारा भी कण्ट्रोल किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्टर के अंदर एक छोटे पंखे को लगाया जाता है। जो LED प्रोजेक्टर को गर्म नहीं होने देता।
3.LCD projector
LCD projector को slide और overhead प्रोजेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रोजेक्टर सपाट सतह पर वीडियो और चित्र को display करता है।
यह किसी इमेज या वीडियो को दिखाने के लिए liquid crystal का इस्तेमाल करता है।
LCD प्रोजेक्टर को maintain करके रखना पड़ता है और समय समय पर इस प्रोजेक्टर को filter की ज़रूरत पड़ती है।
4.Nebula Projector
Nebula Projector को mini प्रोजेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। क्योकि यह एक छोटा portable प्रोजेक्टर है।
यह प्रोजेक्टर wireless होता है। यानी बिना किसी USB डिवाइस की मदद के बिना nebula प्रोजेक्टर को कंप्यूटर के साथ connect किया जा सकता है।
इसके अलावा यह प्रोजेक्टर hd स्क्रीन डिस्प्ले करने की छमता रखता है। Nebula projector वजन में काफी ज्यादा हल्के होते है।
5.Light Projector
light projector को इमेज और वीडियो को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता। बल्कि इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल घर की सजावट के लिए किया जाता है। यानी लाइट प्रोजेक्टर की रौशनी के कारण घर को सजाया जा सकता है।
पुराने समय में लाइट प्रोजेक्टर के अंदर speaker और voice control की सुविधा नहीं होती थी। लेकिन लाइट प्रोजेक्टर के नए version में speaker और voice control की सुविधा उपलब्ध है।
इसके अलावा लाइट प्रोजेक्टर में चमक को कण्ट्रोल किया जा सकता है। यानी user अपने अनुसार लाइट को set कर सकता है।
Advantage of Projector – प्रोजेक्टर के फायदे
1- projector छोटे आकार वाली images और video को बड़े आकार में डिस्प्ले करने की छमता रखता है।
2- प्रोजेक्टर की मदद से student आसानी से किसी भी concept को समझ सकता है।
3- इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार इमेज और वीडियो का size बड़ा छोटा कर सकते है।
Disadvantages of Projector – प्रोजेक्टर के नुकसान
1- इसको maintain करके रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है।
2- इसको चलाने के लिए dark room (अंधेर कमरे) की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी स्थान या कमरे में प्रोजेक्टर को चलाया नहीं जा सकता।
3- इसमें sound के लिए अलग से ऑडियो सिस्टम लगाना पड़ता है।
Speaker (स्पीकर क्या है?)
- Speaker एक आउटपुट डिवाइस है जो sound (ध्वनि) को उत्पन्न करता है।
- स्पीकर को चलाने के लिए sound card की ज़रूरत पड़ती है।
- स्पीकर को computer के साथ कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ , USB और wifi का इस्तेमाल किया जाता है।
- स्पीकर काफी हल्के डिवाइस होते है जो अलग अलग size में उपलब्ध है।

Types of Speaker – स्पीकर के प्रकार
1. Portable Bluetooth speaker
यह speaker कंप्यूटर डिवाइस के साथ bluetooth की मदद से कनेक्ट होते है। इसके अलावा android मोबाइल , लेपटॉप के साथ भी portable bluetooth speaker को जोड़ा जा सकता है।
यह स्पीकर साइज में काफी छोटे और हल्के होते है। जिसे कोई भी user किसी भी स्थान पर लेकर जा सकता है।
इसके अलावा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर को कोई भी user अपने bag में चिपका सकता है। या कहे अपने bag में टांग सकता है।
2. Wireless Speakers
वायरलेस स्पीकर को कंप्यूटर डिवाइस के साथ connect करने के लिए wifi और bluetooth का इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस स्पीकर साइज में थोड़े बड़े होते है। इसके अलावा इन स्पीकर का वजन थोड़ा ज्यादा होता है।
3. Built-in Speakers
Built-in speaker का उपयोग स्टीरियो सेट, टीवी, लैपटॉप और अन्य electronic डिवाइस में किया जाता है।
यह स्पीकर ज्यादा मात्रा में ध्वनि को उतपन नहीं कर सकते। क्योकि built in speaker में ध्वनि उतपन करने की एक सीमा होती है। यह स्पीकर आकार में छोटे होते है और कम वजन वाले होते है।
4.Subwoofer
यह कम frequency वाला स्पीकर है। जिसकी आवाज लगभग 80 hertz की है। Subwoofer में ध्वनि को tracks में capture किया जाता है। subwoofer को कम bass वाली frequency के लिए डिज़ाइन किया गया है।
5.Woofer
woofers का उपयोग ज्यादातर home cinema में किया जाता है। woofers लगभग 80 से 1000 hertz ध्वनि को उतपन करने की छमता रखते है। woofers इस्तेमाल loudspeaker के रूप में भी किया जाता है।
woofers आकार में बड़े होते है। इसके अलावा वूफर्स बहुत ज्यादा मात्रा में ध्वनि उतपन कर सकते है। user अपने इच्छा अनुसार ध्वनि को कम या ज्यादा कर सकता है।
Advantage of speaker – स्पीकर के फायदे
1- स्पीकर के द्वारा हम आवाज को आसानी से सुन सकते है।
2- इसकी मदद से एक ही समय मे बहुत सारें लोग आवाज को सुन सकते हैं।
3- इसको लैपटॉप , मोबाइल, या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करना काफी ज्यादा आसान होता है।
Disadvantages of Speaker – स्पीकर के नुकसान
1- यह बहुत ज्यादा आवाज करते हैं जिससे कुछ लोग इससे परेशान होने लगते है।
2- इसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में noise pollution (ध्वनि प्रदूषण) होता है।
3- इसमें कई बार connectivity issues आने लगते है। यानी कई बार ऐसा होता है की स्पीकर डिवाइस के साथ connect नहीं होता।
4- कुछ ऐसे स्पीकर होते हैं जिनका size काफी बड़ा होता है जैसे कि – शादी में use होने वाले स्पीकर। इन speakers को किसी एक स्थान पर लाने में बहुत दिक्कत होती है।
Headphone (हैडफ़ोन क्या है?)
- Headphone एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल आवाज या गानों को सुनने के लिए किया जाता है। इसे कभी-कभी earphone भी कहा जाता है।
- इसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। इसमें छोटे-छोटे दो स्पीकर लगे होते हैं।
- Headphone का आकार काफी ज्यादा छोटा होता है। इसके अलावा हैडफ़ोन का वजन काफी हल्का होता है। headphone को किसी भी स्थान में लेकर जा सकते है।

Types of Headphone – हैडफ़ोन के प्रकार
1.Closed Back Headphone
Closed back headphone का उपयोग शोर को रोकने के लिए किया जाता है। यानी user इस headphone का इस्तेमाल बाहरी ध्वनि के बचाव के लिए करता है।
यह headphone आकार में छोटे होते है। इसके अलावा closed back headphone ज्यादा expensive (महँगे) नहीं होते।
2.Open-Back Headphones
Open back headphone खुली और हवादार ध्वनि produce करते है। इस हैडफ़ोन में बाहरी सतह पर छोटे छोटे छेद होते है। जिसके कारण open back headphone में हवा cross (आर-पार) हो सकती है।
3.On Ear Headphone
On ear headphone आकार में थोड़े छोटे होते है। इसके अलावा इनका वजन भी काफी हल्का होता है। ऑन एअर हैडफ़ोन को Supra-aural headphone के रूप में भी जाना जाता है। यह headphone यूजर के लिए काफी comfortable होते है। क्योकि दुसरे headphones की तुलना में इसका आकार छोटा होता है।
Advantage of Headphone in Hindi – हैडफ़ोन के फायदे
1- हैडफ़ोन user को बाहरी ध्वनि यानी शोर शराबे से बचाता है।
2- ये ज्यादा expensive नहीं होते।
3- इसको किसी भी स्थान में लेकर जाया जा सकता है।
Disadvantage of Headphone – हैडफ़ोन के फायदे
1- इसकी ध्वनि (sound) सिमित (limited) होती है अर्थात ये ज्यादा तेज आवाज पैदा नही कर सकते।
2- इसकी वजह से कान में infection होने का खतरा बना रहता है।
3- ज्यादा headphone के उपयोग से कान में दर्द होने लगता है।
Sound card (साउंड कार्ड क्या है?)
- साउंड कार्ड एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसको कंप्यूटर की मदरबोर्ड में insert किया जाता है। साउंड कार्ड की मदद से कंप्यूटर की आवाज को बेहतर बनाया जाता है जिससे कि यूजर आवाज को आसानी से सुन सके।
- साउंड कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर game खेलने, music सुनने या मूवी देखने के लिए किया जाता है।
- Sound card दो प्रकार के होते हैं – Internal और External.
- सबसे पहले साउंड कार्ड का अविष्कार 1972 में Sherwin Gooch ने किया था।
- साउंड कार्ड को audio adapter भी कहा जाता है।

Video card (वीडियो कार्ड क्या है?)
- वीडियो कार्ड एक output device है जो कि मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। इसकी मदद से वीडियो और ग्राफ़िक्स की quality को बढ़ाया जाता है।
- वीडियो कार्ड का ज्यादातर इस्तेमाल game खेलने के लिए किया जाता है।
- आजकल के कंप्यूटर में वीडियो कार्ड पहले से ही मौजूद होता है इसलिए हमें इसे खुद से डालने की जरूरत नही पड़ती।
- वीडियो कार्ड बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं इसलिए इसमें heat sink की जरूरत पड़ती है।
- Video card को Graphics card भी कहते हैं।

GPS (जीपीएस क्या है?)
- GPS का पूरा नाम global positioning system होता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से डिवाइस की location का पता लगाया जाता है।
- यह रेडियो पर आधारित navigation system है जो किसी location (स्थान) का पता लगाने के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है।
- GPS में 24 satellite होती है।
- आजकल हमारे फ़ोन में google map होता है जिसकी मदद से हम किसी भी स्थान पर आसानी से जा सकते हैं।


.jpg)



0 टिप्पणियाँ